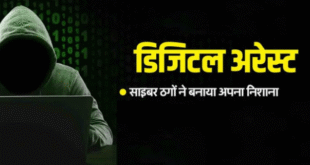“हिंदी दिवस” के बहाने हर साल हम सब उसी पुराने झुनझुने को बजाते हैं,, हिंदी हमारी आत्मा है, हिंदी हमारी पहचान है, हिंदी की जय हो। और अगले ही पल फाइलें, आवेदन पत्र, आदेश और अदालती कार्यवाही अंग्रेज़ी में ही चलती रहती हैं। यह वही स्थिति है, जिसे कवि भवानीप्रसाद मिश्र ने बरसों पहले कहा था,
“हिंदी का दुखड़ा कोई सुनता नहीं, और गाता हर कोई है।”
भारत की इस दुविधा पर याद आता है संस्कृत वचन—
“मातृभाषा न त्याज्या कदापि” अर्थात मातृभाषा कभी भी त्यागने योग्य नहीं।
लेकिन हम भारतीय शायद अपवाद साबित होने पर ही गर्व करते हैं।
आंकड़े चीखते हैं, पर हम बहरे हैं : भारत में 46 करोड़ लोग हिंदी मातृभाषा के रूप में बोलते हैं। विश्व स्तर पर हिंदी बोलने वालों की संख्या लगभग 60 करोड़ से अधिक मानी जाती है। गूगल की 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट पर हिंदी सामग्री की हिस्सेदारी केवल 0.1% है, जबकि अंग्रेज़ी का हिस्सा 55% से अधिक है। शिक्षा मंत्रालय के आँकड़े कहते हैं कि उच्च शिक्षा के 85% से अधिक शोधपत्र आज भी अंग्रेज़ी में लिखे जाते हैं।
सवाल यह है कि इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद हिंदी ज्ञान-विज्ञान और तकनीक की भाषा क्यों नहीं बन पा रही?
राजभाषा, पर राज किसी और का : हिंदी 1950 से भारत की राजभाषा घोषित है। पर सच्चाई यह है कि संसद, न्यायालय, विश्वविद्यालय और बड़े वैज्ञानिक संस्थान अभी भी अंग्रेज़ी की दासता से मुक्त नहीं हुए। क्या यह विडंबना नहीं कि देश का प्रधानमंत्री हिंदी में बोलता है, पर उसी के मंत्रालयों के आदेश अंग्रेज़ी में लिखे जाते हैं?
यह वही दोमुंही स्थिति है जिसे अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार संसद में कहा था—
“राजभाषा हिंदी है, पर राज अंग्रेज़ी करता है।”
दुनिया से सीखने की ज़रूरत : यहाँ पर मुझे अपने हाल की रूस यात्रा का अनुभव जोड़ना होगा। हर तरफ से साधन-संपन्न होने के बावजूद रूस ने तमाम वैश्विक दबाव और आंतरिक कठिनाइयों के बीच अपनी भाषा पर अटूट विश्वास रखा है। विज्ञान हो या परमाणु तकनीक, साहित्य हो या अर्थशास्त्र, हर विषय की पढ़ाई-लिखाई वे अपनी ही भाषा में करते हैं।
इसी तरह जर्मनी और फ्रांस तो भाषा-गौरव के लिए पहले से विख्यात हैं। किंतु मैंने अपनी यात्राओं के दौरान यह भी देखा कि थाईलैंड और कंबोडिया जैसे छोटे देश, और यहाँ तक कि इथियोपिया जैसा सबसे गरीब माने जाने वाला देश भी, अपना सारा शासकीय कामकाज और शिक्षा अपनी भाषा में ही करते हैं। और हम? हम अभी भी सोचते हैं कि हिंदी में विज्ञान पढ़ाने से छात्र “कमजोर” हो जाएंगे!
साहित्य से सॉफ़्टवेयर तक : विश्व हिंदी सम्मेलन, अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस, और हिंदी सप्ताह मनाने की परंपराएँ अब रस्मअदायगी से आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। जबकि आँकड़े बताते हैं कि बॉलीवुड फिल्मों और हिंदी गीतों की वजह से विश्व के लगभग 80 देशों में हिंदी-समझने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अमेरिका, कनाडा, मॉरीशस, फिजी और खाड़ी देशों में हिंदी-भाषी समाज बड़ी ताकत बन चुका है।
फिर भी विज्ञान, तकनीक और न्यायपालिका में हिंदी का स्थान हाशिए पर है।
आखिर दोष किसका? : दोष केवल अंग्रेज़ी या तथाकथित “औपनिवेशिक मानसिकता” का नहीं है। दोष उन नेताओं, नौकरशाहों और शिक्षा-नीति निर्माताओं का है, जो जनता से हिंदी में वोट तो माँगते हैं, पर अपने बच्चों को अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल भेजते हैं।
गांधीजी ने चेताया था:
“किसी राष्ट्र की आत्मा उसकी भाषा में बसती है।”
पर हमने आत्मा को गिरवी रखकर शरीर को बेच दिया है।
भविष्य : अभी भी उम्मीद बाकी
यदि चीन, जापान, रूस, जर्मनी, फ्रांस जैसे देश अपनी भाषा में तकनीकी शिक्षा और शासन चला सकते हैं, तो भारत क्यों नहीं? हिंदी न केवल भारत में, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक मज़बूत दावेदार बन सकती है—बशर्ते हम इसे विज्ञान, तकनीक और प्रशासन की मुख्यधारा में लाएँ।
हिंदी का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि यह केवल “भावना” की भाषा रहेगी या “ज्ञान” की भी भाषा बनेगी।
सम्प्रति- लेखक डॉ.राजाराम त्रिपाठी स्वतंत्र स्तंभकार तथा जनजातीय सरोकारों की हिन्दी मासिक पत्रिका के सम्पादक हैं।
 CG News | Chhattisgarh News Hindi News Updates from Chattisgarh for India
CG News | Chhattisgarh News Hindi News Updates from Chattisgarh for India