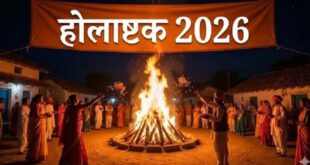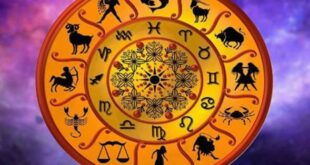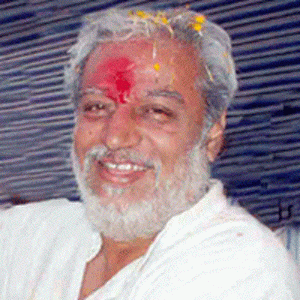
किसानों और खेती की स्थिति लगभग हर वर्ष पीड़ा दायक रहती है, क्योंकि कृषि लगभग प्रकृति पर निर्भर है। किसानों और कृषि क्षेत्र के समक्ष निम्न प्रकार के संकट आते हैं :-
- सूखा, 2. बाढ़़, 3. ओलावृष्टि, 4. अति वृष्टि, 5. कीड़ों का प्रकोप, 6. तुषार (पाला),
शायद ही कोई ऐसा वर्ष गुजरता हो जब किसान इन प्राकृतिक आपदाओं में से किसी न किसी प्रकार के संकट का शिकार न होता हो। वैसे तो सभी प्रकृति प्रदत परेशानियाँ है, परन्तु इनमें से कुछ का इलाज सीधे तौर पर व्यवस्था के माध्यम से संभव है।
सूखा और बाढ़ एक सिक्के के ही दो पहलू है, और अगर देश की व्यवस्था, व राजनीति ने गाँव के विकास को अपना लक्ष्य बनाया होता तथा बाढ़ के पानी को नहरों के माध्यम से सूखाग्रस्त इलाको तक पहुँचाने की व्यवस्था की होती, तो कम से कम इन दो व्याधियों से देश को मुक्ति मिल सकती थी।
स्व. डॉ. राम मनोहर लोहिया ने तो लगभग 70 वर्ष पूर्व यह प्रस्ताव सरकार के सामने रखा था कि सूखा और बाढ़ नामक जुड़वा बीमारियों से नदियों को जोड़कर तथा नहरों का जाल बिछा कर मुक्ति दिलायी जा सकती थी, परन्तु उनके इस प्रस्ताव को न तो तत्कालीन भारत सरकार ने माना, बल्कि परवर्ती सरकार ने भी डॉ. लोहिया की बात को अनसुना कर दिया। स्व. अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने अवश्य तात्कालीन जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश प्रभु के माध्यम से इस विषय पर कुछ पहल की थी, परन्तु योजना बहुत आगे नहीं जा सकी। कीटनाशक आदि की समस्या का कुछ हल कीट नाशकों के प्रयोग से निकाला जा रहा है, यद्यपि इस क्षेत्र में बहुत दूर तक हल नजर नहीं आ रहा है, एक तो इसलिए कि कीटनाशकों के भारी प्रयोग से न केवल जमीनों की गुणवत्ता समाप्त हो रही है, बल्कि कीटनाशकों का जहर अब जमीन को भी जहरीला बना रहा है, दूसरी तरफ कीटनाशक रवाद्यान और सब्जियों में इतना अधिक प्रभाव डालने लगा है जिससे खाद्यान और सब्जियों मानव जाति के लिए जहर खाने जैसा खतरनाक होने लगी है। चूंकि किसान को अपने जीवनयापन के लिए पैसा चाहिए, उसको फसलों का अधिक उत्पादन चाहिए, अतः वह नीति-अनीति, या तात्कालिक सवालों पर सोचे बिना कीटनाशकों का इस्तेमाल कर रहा है। जीवन जीने की इच्छा के कारण यह उसकी एक लाचारी जैसी बन गई है। आबादी की वृद्धि इतनी अधिक हो गई है, कि अगर अब तत्काल लोग, किसान या समाज गोबर खाद पर जाना चाहे तो गोबर खाद के प्रयोग के कारण उसकी पैदावार की मात्रा बहुत घट जाएगी और वह ठीक से अपना परिवार का जीवनयापन भी नहीं कर सकेगा।
इसी प्रकार अतिवृष्टि, ओला और पाले का कोई वैधानिक इलाज फिलहाल तो नज़र नहीं आता है। प्रकृति का बढ़ता असंतुलन इसका मुख्य कारण लगता है, और इस असंतुलन को नियंत्रित करना यद्यपि आंशिक रूप से मानव के हाथ में है, परन्तु पूर्ण रूप से नहीं है।
लगभग हर वर्ष कोई न कोई प्राकृतिक विपत्ति कृषि और किसानों को अपना शिकार बनाती है, जैसे इस बारिश के मौसम में म.प्र. के लगभग आधे से अधिक इलाकों में अतिवृष्टि से उरद और सोयाबीन की फसलें नष्ट हो गई है, किसानों के द्वारा लगाई गई लागत जो खाद, बीज, दवा आदि में लगायी गई थी वह भी नष्ट हो गई, खेतों में पानी भरा पड़ा है, उरद और सोयाबीन के पौधे की जड़ें गल चुकी है, और वे खेत कब तक अगले गेंहू की फसल बोने लायक हो सकेंगे आज कहना कठिन है। पिछले वर्ष इसी प्रकार प्रदेश के बड़े इलाके में अतिवृष्टि व ओले दोनों से बर्बादी हुई थी और इस प्रकार की घटनाओं के परिणामस्वरूप अन्ततः किसान कर्जदार बन जाता है, उसे अगले फसल की तैयारी के लिए खाद बीज चाहिए, अपने जीवन जीने का खर्च चाहिए, यह सब उसे कर्ज लेकर ही पूरा करना पड़ता है, यही वजह है कि, कर्जदार किसानों की संख्या घटने की बजाय बढ़ती चली जाती है। वैसे तो सरकार ने के.सी.सी. यानि किसान क्रेडिट कार्ड के नाम से बड़े पैमाने पर कर्ज देने की व्यवस्था बनाई है, और पुराने सख्त नियमों को काफी शिथिल भी किया है, पर इसके बावजूद भी किसानों के सामने कर्ज की लाचारी पैदा हो जाती है। अब मान लीजिए किसी किसान को अपने परिजन की गंभीर बीमारी से निपटना हो, बेटी के हाथ पीले करना हो, तो वह यह सब किस प्रकार की व्यवस्था से करें, क्योंकि किसान को शीघ्र और फौरी तौर पर अपनी व्यवस्थाओं के हल करने की उम्मीद जिससे थी, वे सब गड़बड़ा गए है। कई बार किसान स्वतः भी लालच में या परिवार के बच्चों के दबाव में गैर कृषि कार्यों के लिए कृषि के नाम पर ऋण ले लेता है, और उसे चुका नहीं पाता। अपनी क्षमता भर सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंको से ऋण लेने तथा ऋण सीमा पार करने के बाद वह निजी साहूकारों की तरफ बढ़ता है और उल्टी सीधी दरों पर याने भारी ब्याज पर वह निजी साहूकारों से कर्ज ले रहा है। पिछले कुछ दशकों से किसानों की कर्जमाफी का नारा राजनैतिक क्षेत्रों में हुआ है, कृषि को लेकर 60 के दशक से हम समाजवादी यह नारा लगाते रहे कि देश में समान नीति होना चाहिए और जिस प्रकार उद्योग क्षेत्र, घाटेवाले, बीमार कारखानां का कर्ज सरकारें माफ करती है, या उन कर्जां को एन.पी.ए. में डाल देती है, उसी प्रकार किसानों का भी कर्ज माफ होना चाहिए। इस नारे का परिणाम भी हुआ और 80 के दशक के अंत से किसानों की कर्ज माफी देश के किसानों का एक प्रमुख कार्यक्रम बन गया। 1989 में जनता दल की केन्द्र सरकार ने 10 हजार तक के कर्ज वाले किसानों के कर्जमाफ किए थे, कालांतर में राज्यों में भाजपा सरकार ने, फिर केन्द्र में यू.पी.ए. सरकार ने, और अभी हाल में म.प्र., छत्तीसगढ., राजस्थान और पंजाब की सरकारों ने किसानों के कर्जमाफी के कार्यक्रम घोषित किए और कुछ कर्ज माफ भी किए। इसके बावजूद भी किसानों की कर्जदारी में कोई विशेष अंतर नहीं आया, इन कारणों को समझना है।
प्राकृतिक विपदा के अलावा निम्न कारण भी है, जो किसानों को कर्जदार बनाते हैं।
- किसानों को फसलों का उचित दाम ना मिलना।
- फसलों के बीज का असंतुलित उतार-चढ़ाव।
- फसल बीमा या कृषि बीमा की कार्यप्रणाली का गलत हेना और बीमा क्षेत्र का निजीकरण होना।
जहाँ तक पहले बिन्दु का प्रश्न है, किसान को फसलों के दाम तय करने के लिए सरकारों ने एक तरफ न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने की नीति बनायी है, परन्तु इसका कोई तार्किक या वैज्ञानिक आधार नहीं है। यह प्रचार किया जाता है, कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में फसलों के दाम तय करने का सिद्धांत बनाया गया है, हालांकि स्वामीनाथन आयोग ने कृषि उपज मूल्य तय करने के जो आधार बताए है, इसमें कोई नया नहीं है, बल्कि डॉ. लोहिया के दामबांधो सिद्धांत का ही दोहराव है, और वह भी अधूरा। डॉ. लोहिया ने 60 के दशक में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि किसानों और बाजार की वस्तुओं का लागत मूल्य निकाला जाना चाहिए उसमें 50 प्रतिशत और जोड़कर किसानों और बाजार के उत्पाद का दाम तय किया जाए। यह दामबांधो नीति कृषि और कारखानों दोनों पर समान रूप से लागू होना चाहिए। परन्तु स्वामीनाथन ने केवल कृषि क्षेत्र को तो इस सिद्धांत से बांधा और बाजार के उत्पाद को खुला छोड़ दिया। परिणाम यह है कि, जो थोड़े बहुत दाम किसान को ज्यादा मिलेंगे उससे कई गुना ज्यादा पैसा उसे बाजार की वस्तुओं इत्यादि खरीदने में खर्च करने पड़ते हैं, क्योंकि स्वामीनाथन बाजार पर रोक लगाने की चर्चा नहीं करते, यह एक प्रकार से कृषि क्षेत्र पर पूँजीवादी सिद्धांत है।
कृषि बीमा, उद्योग तथा बाजार के बीमा में, बुनियादी फर्क है तथा कृषि क्षेत्र के विपत्ति पीड़ित के बीमा में वास्तविक क्षति के अनुकूल क्षतिपूर्ति मिल सके ऐसा कोई प्रावधान नहीं। इतना ही नहीं भारत सरकार ने जो बीमा के क्षेत्र में देशी-विदेशी निजी पूँजीपतियों को अवसर दिया है, यह और भी खतरनाक है। यह कम्पनियाँ लगभग सरकारी दबाव से परे है, और किसानों को सिवा बीमा के प्रीमियम जमा करने के, क्षतिपूर्ति पाने का कोई रास्ता नहीं है। बहुत सारी बीमा कम्पनियों किसानों का पैसा लेकर भाग गई और सरकारें उनके सामने लाचार है।
चूंकि किसानों के पास बाजार नहीं है अतः वे बाजार में लुटने को लाचार है जबकि किसान की फसल आती है तो षड़यंत्रपूर्वक फसलों के दाम एक दम गिर जाते है तथा जब किसान की फसल बिक जाती है, तो उन्हीं फसलों के दाम बाजार में आसमान पर पहुँच जाते है। डॉ. लोहिया ने सुझाव दिया था कि दो फसलों के बीच का उतार चढ़ाव 6 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए अगर यह नीति बन जाए तो एक तरफ किसानों को वाजिब दाम मिलेंगे और दूसरी तरफ आम उपभोक्ता बाजार की लूट से बच जायेंगे।
परन्तु इन मुद्दों पर सरकारों के नीति निर्माताओं के पास कोई विचार नहीं है। एक विचित्र सी स्थिति है कि, किसान भ्रमित और मूक है, बाजार संबल है, तथा राजनीति धन की दासी बन गई है। किसानों के छुटपुट आंदोलन या एक दो हिंसक घटनाओं के आंदोलन से कोई परिणाम न हासिल हुआ है और न होगा। सरकारें कभी-कभी किसानों के आक्रोश की शिकार होगी, सरकार बदल जाएगी परन्तु नीतियां, शोषण और अन्याय जस का तस बना रहेगा। किसानों को अब अपने वोट का इस्तेमाल चहेरा बदलने के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था बदलने के लिए करना होगा, वर्ना मरते रहे है, और मरते रहेंगे, हत्यारी व्यवस्था के हाथों खेले जाते रहेंगे।
सम्प्रति – लेखक श्री रघु ठाकुर देश के जाने माने समाजवादी चिन्तक एवं लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के संस्थापक है।
 CG News | Chhattisgarh News Hindi News Updates from Chattisgarh for India
CG News | Chhattisgarh News Hindi News Updates from Chattisgarh for India