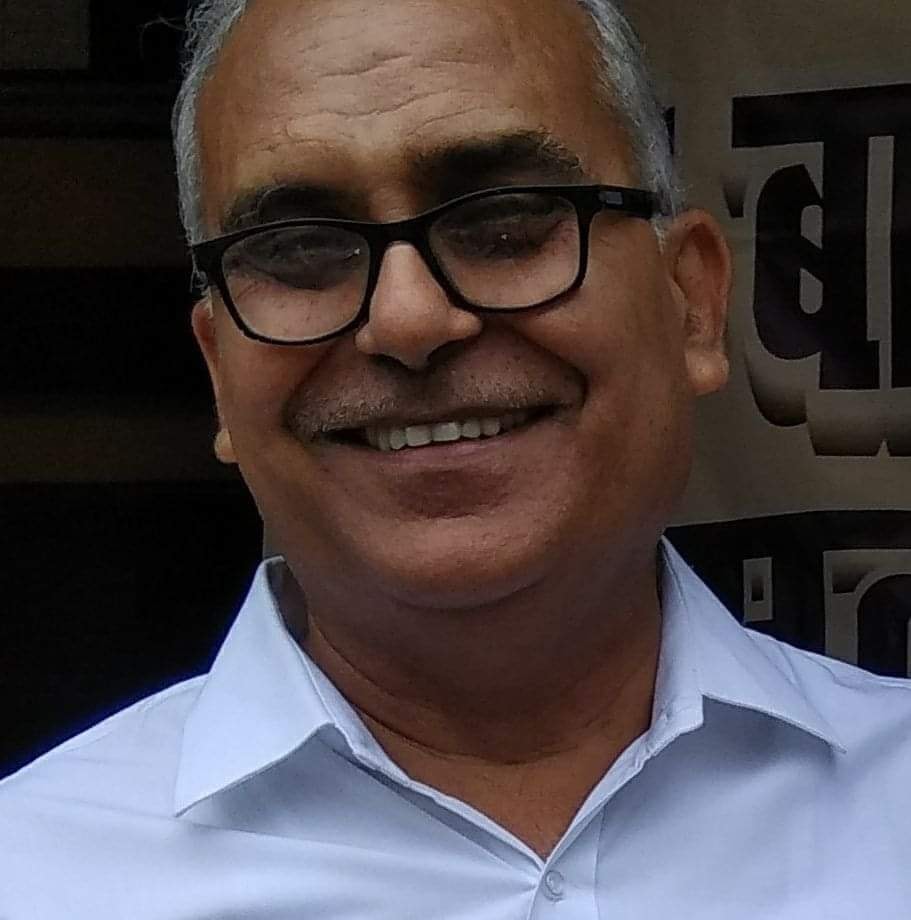
हाईकोर्ट अपना फैसला दे चुका था। अब सबकी निगाहें इंदिराजी के जबाब पर थीं। विपक्ष इस्तीफे का दबाव बढ़ा रहा था। तो समर्थक चुनाव में मिले विपुल जनादेश का हवाला दे रहे थे। दिल्ली के साथ ही पड़ोसी राज्यों से आने वाले या फिर लाये जाने वाले हुजूम 1 सफदरजंग पर जुटकर मरने-मिटने की कसमें खा रहे थे। वफ़ादारी की होड़ में पार्टी नेता और राज्यों के मुख्यमंत्री सब शामिल थे। किसी कड़े कदम की आहट थी। पर वह क्या होगा ? क्या यह हालात सिर्फ 12 जून के इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले की देन थे, जिसने इंदिराजी का रायबरेली से लोकसभा का निर्वाचन रद्द करके अगले छह साल के लिए उन्हें किसी संवैधानिक पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था ?
1969 के कांग्रेस के ऐतिहासिक विभाजन के बाद इंदिराजी ने समय से पहले जनता की अदालत में जाने का फैसला किया था। इससे पहले 1967 में लोकसभा चुनाव हुए थे। उस चुनाव में लोकसभा में कांग्रेस को 283 सीटें प्राप्त हुई थीं, जो कि 1962 की तुलना में 78 कम थीं। उससे भी बड़ा झटका पार्टी को राज्यों के विधानसभा चुनाव में लगा था। तब नौ राज्यों में गैरकांग्रेसी संविद की सरकारें बन गई थीं। दिसम्बर 1970 में लोकसभा भंग करने के बाद 1971 में इंदिराजी गरीब समर्थक प्रगतिशील छवि के साथ जनता के बीच पहुँची थीं। 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण और पूर्व रियासतों के राजाओं के प्रिवीपर्स खात्मे के बाद उनकी लोकप्रियता में जबरदस्त बढोत्तरी हुई थी। कांग्रेस के विभाजन में उन्होंने पुराने दिग्गजों को किनारे लगाकर पार्टी और सरकार पर अपनी पकड़ सिद्ध की थी। 1969 में राष्ट्रपति चुनाव में उनके प्रत्याशी वी.वी.गिरि कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी नीलम संजीव रेड्डी पर जीत दर्ज कर चुके थे। इंदिराजी की लोकप्रियता चरम पर थी। बिखरे विपक्ष ने साझा चुनौती देने का फैसला किया। कांग्रेस (ओ), स्वतंत्र पार्टी , जनसंघ और संसोपा का महागठबंधन ‘ बना। इंदिरा हटाओ उसका नारा था। इंदिराजी का पलटवार , ‘ वे कहते हैं इंदिरा हटाओ – हम कहते हैं गरीबी हटाओ ‘ बहुत मारक साबित हुआ। वोटरों ने इंदिराजी की झोली भर दी। 1967 की तुलना में उन्हें 69 ज्यादा अर्थात 352 सीटें प्राप्त हुईं। महागठबंधन को वोटरों ने पूरी तौर पर नकार दिया। सिंडीकेट कांग्रेस ( ओ) को सिर्फ 16 सीटें मिलीं। 1967 में स्वतंत्र पार्टी को 44 सीटें मिली थीं। इस बार संख्या आठ थी। जनसंघ 35 से घटकर 22 और संसोपा 23 से तीन पर पहुँच गई। चरणसिंह के भारतीय क्रांतिदल को सिर्फ एक सीट मिली। इतना ही काफी नहीं था। इसी साल बांग्ला देश के निर्माण में उनकी साहसिक -निर्णायक भूमिका , पाकिस्तान पर एकतरफा जीत और सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका को ठेंगा दिखाकर देवी दुर्गा का मुकुट इंदिराजी के माथे पर सज चुका था। इस दौर में वह सिर्फ देश की निर्विवाद नेता नहीं थीं। दूसरे देशों ने भी उनके नेतृत्व का लोहा माना था।
पर आगे उतार की रपटीली ढलान थी। बांग्लादेश का निर्माण शोहरत और पाकिस्तान से हिसाब चुकता करने का मौका लाया तो त्रासदियों का कारण भी बना। वहाँ से आये एक करोड़ से ज्यादा शरणार्थियों का बोझ देश पर आया। 1972 से लगातार तीन साल तक सूखा पड़ा। अनाज उत्पादन आठ फीसद घट गया। कीमतों में जबरदस्त उछाल आया। खाद्यान्न के थोक व्यापार को सरकार ने हाथों में लिया और फिर समस्याएं बढ़ते ही उससे पिंड छुड़ाया। खाद्यान्न व्यापार के राष्ट्रीयकरण की अफवाह के बीच खाद्यान्न बाजार से गायब होने लगे। देश के अनेक हिस्सों में खाद्यान्न की लूट की घटनाएं हुईं। तेल निर्यातकों के संगठन ओपेक ने कच्चे तेल के दामों में चार गुनी तक वृद्धि की , जिसका सीधा असर वस्तुओं की कीमतों पर आया। 1974 आने तक महंगाई की दर तीस फीसदी को छूने लगी। औद्योगिक अशांति, कारखानों की बंदी , श्रमिक हड़ताल इन सबका सीधा असर जनजीवन पर पड़ा। 1972-73 में अकेले बम्बई में 12 हजार हड़तालें हुईं। बेरोजगारी का दायरा और बढ़ा। 1974 में जार्ज फर्नांडिस की अगुवाई में 14 लाख कर्मचारियों की रेल हड़ताल को यद्यपि केंद्र ने जल्दी ही सख्ती से कुचल दिया लेकिन इसने सरकार के खिलाफ एक और बड़े वर्ग को लामबंद कर दिया। सत्तादल को अब सरकार के प्रगतिशील उपायों में न्यायपालिका बाधक नजर आने लगी थी। पार्टी के भीतर वामपंथी रुझान के स्वरों ने प्रतिबद्ध न्यायपालिका की जरूरत का राग छेड़ दिया। अप्रैल 1973 में इसी कोशिश के तहत सर्वोच्च न्यायालय के तीन न्यायधीशों जस्टिस हेगड़े, जस्टिस शेलेट और जस्टिस ग्रोवर की वरिष्ठता को अतिक्रमित करके जस्टिस ए. एन. रे को मुख्यं न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया। इंदिराजी का मन संसदीय कार्यवाही से उचटने लगा था। कम्युनिस्ट नेता हीरेन मुखर्जी ने 1973 में लिखा , ‘ उनके पिता संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेकर खुश होते थे , जबकि इंदिराजी उससे उदासीन नजर आती हैं। कभी-कभी लगता है कि वह राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार तो नहीं चाहतीं ? ‘ इस संकट के बीच इंदिराजी ने दो बड़े साहसिक कदम उठाए। 18 मई 1974 को देश ने पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया। उधर 8 अप्रैल 1975 को सिक्किम के चोग्याल को उनके महल में नजरबंद कर दिया गया। सिक्किम का भारत में विलय हो गया और वह देश का 22वां प्रदेश बन गया। अन्य किसी समय में यह दो बड़े काम प्रधानमंत्री को देश के भीतर बेहद लोकप्रिय बनाकर और मजबूत करते। लेकिन आंतरिक अशांति और बेकाबू जन समस्याओं के बीच ये बड़ी उपलब्धियाँ भी अनुकूल राजनीतिक असर नहीं दिखा सकीं।
सरकार और विपक्ष की कटुता बढ़ रही थी। इंदिराजी को हर समस्या के पीछे विदेशी और विपक्ष की साजिश नजर आ रही थी। उनके हर भाषण में जोर-शोर से विपक्ष पर हमले होते। 1971 के चुनाव में साफ हो गए विपक्ष को फिर से खड़ा होने का मौका मिल रहा था। 1974 के जबलपुर लोकसभा उपचुनाव में साझा विपक्ष के प्रत्याशी शरद यादव की जीत ने विरोधी दलों का हौसला बढ़ाया। लेकिन उसे असली ताकत गुजरात के छात्र आंदोलन ने दी। 20 दिसम्बर 1973 को एल. डी. इंजीनियरिंग कालेज के छात्र मेस खर्च में 20 फीसद बढोत्तरी के खिलाफ सड़कों पर उतरे। 3 जनवरी 1974 को हड़ताल में गुजरात विश्विद्यालय के छात्र भी शामिल हो गए। 7जनवरी को पूरे प्रदेश के छात्र सड़कों पर थे। फिर इसमें श्रमिक, मध्यवर्ग, वकील, शिक्षक सब जुड़ते गए और नई मांगें शामिल होती गईं। 10 जनवरी से दो दिन के लिए अहमदाबाद और बड़ोदरा बंद रहा। 25 जनवरी को प्रांतव्यापी हड़ताल के दौरान 33 शहरों में हिंसक टकराव हुआ। सेना बुलानी पड़ी। 44 शहरों में कर्फ्यू लगा। भ्रष्टाचार और नाकामियों से घिरी गुजरात की चिमनभाई पटेल सरकार आंदोलनकारियों के निशाने पर थी। महीने भर के भीतर हिंसक वारदातों में लगभग 100 जानें गईं। 3000 से ज्यादा घायल हुए। 8000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुईं। इंदिराजी को चिमनभाई को इस्तीफे के लिए कहना पड़ा। 9 फरवरी को उन्होंने इस्तीफा दिया। केंद्र को अपने ही दल द्वारा शासित राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। ऐसा राज्य जिसकी 167 सदस्यीय असेम्बली में कांग्रेस के 140 सदस्य चुन कर आये थे। 11 फरवरी को जेपी गुजरात पहुँचे। छात्रों- युवाओं का जोश और बढ़ा। आंदोलन की ताकत और दबाव विधायकों के इस्तीफों से परखा जा सकता है। 16 फरवरी को कांग्रेस (ओ) के 15 विधायकों ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया। फिर इसमें जनसंघ के तीन विधायक जुड़े। आखिर तक छात्रों ने 95 विधायकों को इस्तीफे के लिए मजबूर कर दिया। 12 मार्च 1974 को 79 साल के मोरारजी देसाई असेम्बली भंग करने की मांग लेकर अहमदाबाद में आमरण अनशन पर बैठ गए। 16 मार्च को असेम्बली भंग करनी पड़ी। 6 अप्रैल 1975 को मोरारजी भाई एक बार फिर से अनशन पर थे। इस बार मांग भंग विधानसभा के चुनाव कराने की थी। 10 जून को चुनाव हुआ। 12 जून को इलाहाबाद हाईकोर्ट के खिलाफ फैसले के बाद इंदिराजी के लिए गुजरात से दूसरी निराश करने वाली खबर थी। पिछले चुनाव की तुलना वहाँ कांग्रेस की 65 सीटें कम हुईं। पार्टी विपक्ष में पहुँची। राज्य में जनता मोर्चा की बाबू भाई पटेल की अगुवाई में पहली गैरकांग्रेसी सरकार बनी।
गुजरात की आँच दूसरे राज्यों तक पहुँच रही थी। बिहार इसमें आगे था। 18 मार्च 1974 को पटना के छात्र सड़कों पर थे। आह्वान विधानसभा का सत्र न चलने देने का था। कांग्रेस विधायक सुबह ही विधानसभा पहुँच गए। लेकिन छात्रों ने राज्यपाल आर.डी. भंडारे की कार को घेर लिया। इसके बाद पुलिस के लाठी चार्ज -आंसू गैस के गोलों की बरसात के बीच व्यापक हिंसा हुई। छात्रों ने जेपी से अगुवाई की गुजारिश की। लम्बे समय पहले सक्रिय राजनीति से विलग हुए जेपी देश के बिगड़ते हालात से बेचैन थे। इंदिराजी और सांसदों को उन्होंने इस सिलसिले में चिट्ठी भी लिखी थी। उन्होंने छात्रों के सामने राजनीतिक दलों से अलग रहने की शर्त रखी। छात्र राजी हुए। 8 अप्रैल को लाखों की भीड़ पटना की सड़कों पर जेपी के पीछे थी। 5 जून 1974 पटना के गांधी मैदान में उमड़ा जनसैलाब जेपी के ‘ सम्पूर्ण क्रांति ‘ आह्वान का साक्षी बना। जेपी ने कहा कि मंत्रिमंडल के इस्तीफे और विधानसभा भंग होने भर से बदलाव नहीं आएगा। व्यवस्था परिवर्तन जरूरी है। साल भर के लिए कालेज-विश्वविद्यालय बंद करने और छात्रों-युवकों की शक्ति के समाज-राष्ट्र निर्माण में उपयोग की उन्होंने जरूरत बताई। 7 जून से बिहार विधानसभा भंग अभियान शुरू हुआ। जनसंघ के 24 में 13 विधायकों ने सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। नेतृत्व के निर्देश के पालन से इनकार करने वाले 11 विधायक पार्टी से निकाल दिए गए। संसोपा के 13 में सात ने इस्तीफा दिया। कांग्रेस (ओ) के 23 में किसी विधायक ने इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन इस सबसे अलग जेपी की अगुवाई और प्रमुख विपक्षी दलों के जुड़ाव ने आंदोलन को राष्ट्रीय स्वरूप दे दिया। वे जिस राज्य में भी पहुँचे लोग उन्हें सुनने को उमड़ पड़े। वे पंडित जवाहर लाल नेहरू के मित्र रहे थे। उनकी सरकार में शामिल होने या फिर बाद में भी सत्ता से जुड़े हर लाभ को उन्होंने ठुकराया था। उनकी नैतिक सत्ता और आभामंडल किसी भी सत्ता पर भारी था। 4नवम्बर 74 को पटना में जेपी पर उठी पुलिस की लाठियों की चोट नानाजी देशमुख ने झेली। इस खबर से सारे देश में सत्ता विरोधी गुस्सा और प्रबल हुआ। इंदिराजी के कुछ बयानों और उनसे ज्यादा कुछ चाटुकारों की अशोभनीय टिप्पणियों ने जेपी को सीधे संघर्ष के रास्ते पर खींच लिया। उधर सदन में प्रचंड बहुमत के बावजूद सरकार जन असंतोष को थामने में विफल साबित हो रही थी। जेपी की अगुवाई ने इस असंतोष को और प्रबल किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 12 जून के फैसले ने इंदिराजी से शासन का नैतिक हक छीन लिया। फैसले ने विपक्ष को और ताकत दी। डॉक्टर लोहिया याद किये जा रहे थे , ‘ जिंदा कौमें पांच साल इंतजार नहीं करतीं।’ जेपी , दिनकर को दोहरा रहे थे , ‘ सिंहासन खाली करो कि जनता आती है।’ गुजरात की सीख ताजा थी । इंदिराजी अब और झुकने के लिए तैयार नहीं थीं। वह जो कदम उठाने जा रही थीं, उसकी उनके सहयोगियों को भी भनक नहीं थी। 25 जून 1975 की तारीख करीब थी।
सम्प्रति- लेखक श्री राजखन्ना वरिष्ठ पत्रकार है।श्री खन्ना के आलेख देश के प्रतिष्ठित समाचार पत्रों,पत्रिकाओं में निरन्तर छपते रहते है।श्री खन्ना इतिहास की अहम घटनाओं पर काफी समय से लगातार लिख रहे है।
 CG News | Chhattisgarh News Hindi News Updates from Chattisgarh for India
CG News | Chhattisgarh News Hindi News Updates from Chattisgarh for India



